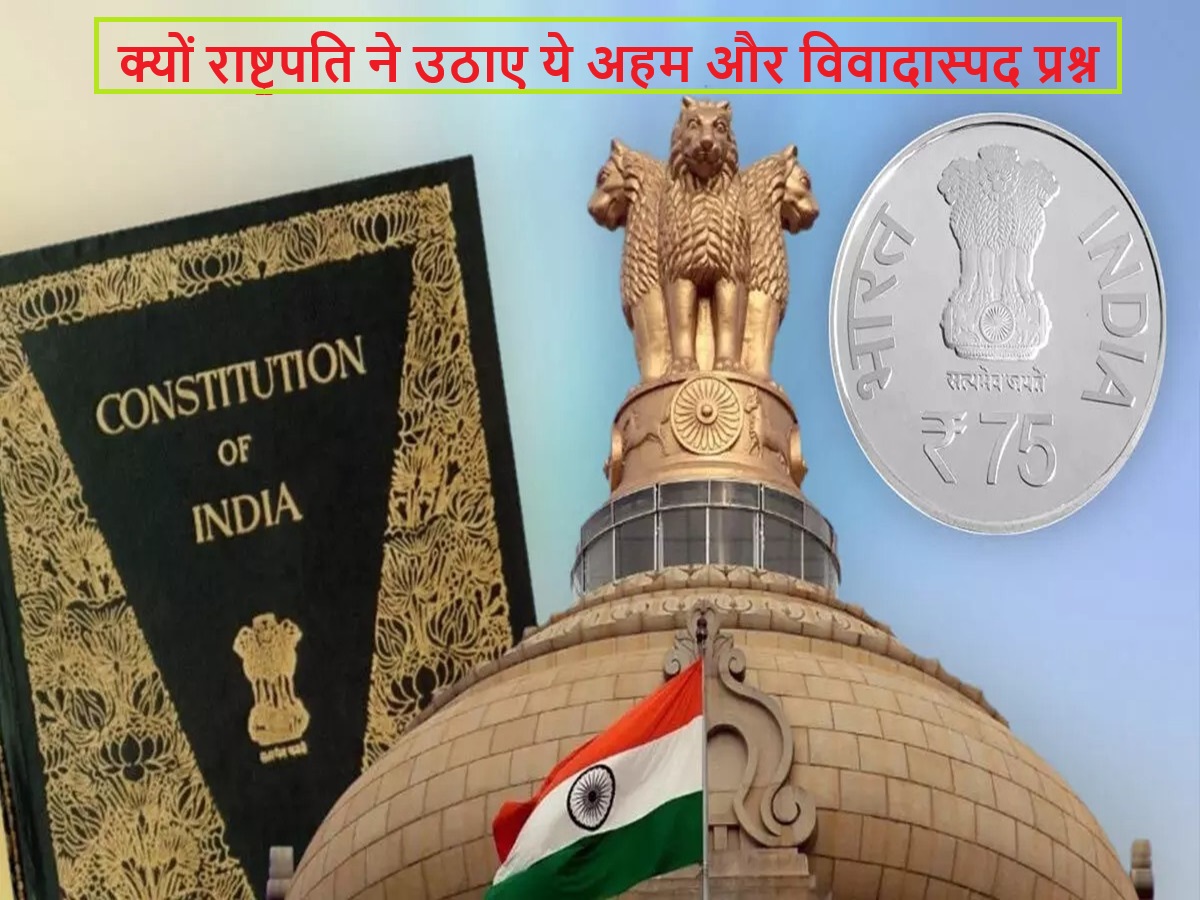
Up Kiran, Digital Desk: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है; इसके लिए संविधान पंडितों को विभिन्न संघर्षों, विवादों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से राज्य और संघ सरकारों के अच्छे और बुरे शासन का अध्ययन करना होगा।
यह संघीय चरित्र का प्रश्न है, जहां 'संघ का नाम और क्षेत्र' के आसपास का पहला अनुच्छेद कहता है कि "(1) इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का संघ होगा। (2) राज्य और उनके क्षेत्र प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे"। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, यह भारत के राज्यों का संघ है, तथाकथित। इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में राज्य सरकार चलाने में राज्यपालों के पास बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं।
राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए सवालों की सूची राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की शक्तियों के इर्द-गिर्द है, खासकर जब भारत में राज्यपाल का चयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रधान मंत्री करते हैं, गृह मंत्री की मदद से और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि वे सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं। राष्ट्रपति ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से क्रमशः राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के कानून के लिए सहमति प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा। ये लेख निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला प्रभावी रूप से राष्ट्रपति और राज्यपालों के कार्यालयों में निहित विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करता है, जिससे मौलिक संवैधानिक चिंताएँ उठती हैं।
राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देशभर में राजभवनों और मुख्यमंत्रियों के बीच बढ़ते टकराव की पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांगी है, क्योंकि कई विधेयकों को उचित समय से अधिक समय तक 'लम्बित' रखा गया है, जिसका प्रभाव राज्यों के शासन पर पड़ रहा है, जिनका प्रशासन केंद्र के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा किया जाता है।
तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2025 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर 'पॉकेट वीटो' शब्द गढ़ा। कोई व्यक्ति 'कार्रवाई' करके शासन कर सकता है और कुछ न करके भी 'निष्क्रियता' कहला सकता है। यदि अधिकांश मंत्री निष्क्रियता से शासन को विफल करते हैं, तो इसका परिणाम अराजकता होगा।
तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि गैर-भाजपा शासित कई राज्य 'निष्क्रियता' से पीड़ित हैं। लोगों को शासन करने का अधिकार है, चाहे वह राज्य हो या केंद्र। राष्ट्रपति 14 सवालों पर स्पष्टीकरण चाहते हैं।
इनमें से पांच सबसे महत्वपूर्ण हैं:
1. क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
2. क्या अनुच्छेद 361 (राष्ट्रपति और राज्यपालों को दी गई उन्मुक्ति) अनुच्छेद 200 के तहत न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है?
3. संविधान के अभाव में राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग की कोई समय-सीमा या तरीका निर्धारित है?
4. क्या अनुच्छेद 201 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग (यदि राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया गया हो) न्यायोचित है?
5. क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति न्यायिक आदेशों के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं?
स्वतंत्रता से पहले, संदर्भित मामलों पर सलाहकार राय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 213(1) में पाई जा सकती है। 1950 के संविधान के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों पर सलाहकार क्षेत्राधिकार था जो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसे सलाहकार क्षेत्राधिकार के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।
अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता है
1. अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किसी विधेयक को स्वीकृति प्रदान करते समय राज्यपाल के समक्ष क्या विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है?
3. क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना आवश्यक है?
4. क्या अनुच्छेद 200 और 201 के अंतर्गत न्यायालयों को न्यायिक निर्णय लेने की अनुमति है?
5. क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपालों की शक्तियों को न्यायिक शक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है?
6. क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है?
7. क्या सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी मामले की जांच करे, जिसमें संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, और अनुच्छेद 145(3) के तहत मामले को न्यूनतम पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजे?
8. क्या अनुच्छेद 142 प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित है या क्या यह “संविधान के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत” निर्देश जारी करने तक विस्तारित है?
9. क्या अनुच्छेद 131 के अंतर्गत मूल वाद दायर करने के अलावा किसी अन्य तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच निर्णय लेने पर सर्वोच्च न्यायालय पर कोई प्रतिबंध है?
एस.सी. की पृष्ठभूमि
एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 10 राज्य विधान विधेयकों को रोकना “अवैध” और “गलत” था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिन विधेयकों पर सहमति लंबित थी और जिन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था, उन्हें मंजूरी मिल गई है।
क्या प्रश्न यह है कि क्या कोई समय-सीमा तय की जा सकती है, या यदि ऐसा है, तो इसमें ऐसी समय-सीमा भी निर्धारित की गई है जिसके भीतर राज्यपाल और राष्ट्रपति को उनके समक्ष रखे गए विधेयकों पर अपने निर्णय की सूचना देनी है?
इसने राज्यपाल के कार्यों के लिए न्यायिक समीक्षा के दायरे को भी बढ़ाया, जिससे राज्य सरकारें अदालतों का रुख कर सकें और इन समयसीमाओं का पालन न किए जाने पर परमादेश रिट की मांग कर सकें। परमादेश रिट एक सक्षम अदालत को किसी सरकारी अधिकारी को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि अनुच्छेद 200 राज्यपाल को तीन विकल्पों में से केवल एक तक सीमित करता है।
राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देते हैं और विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करके उसे वापस भेज देता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि सहमति न देने से राज्यपाल प्रावधान के तहत विकल्पों में से एक को समाप्त कर देते हैं।
उन्होंने लिखा कि राज्यपाल द्वारा सहमति न देने के खिलाफ "एक सख्त संवैधानिक निषेध है।" सुप्रीम कोर्ट ने एक "संभावित परिदृश्य" पर चर्चा की, जहां विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब विधानमंडल किसी विधेयक में नए बदलाव पेश करता है, जिसकी राज्यपाल द्वारा उसे वापस करने के बाद अनुशंसा नहीं की जाती है। ऐसे विधेयक पर "पूरी तरह से अलग और नए आधारों" पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विधेयक को केवल राज्यपाल की सिफारिशों पर संशोधित किया जाता है, तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकते हैं। सब कुछ 'सिर्फ' सलाहकार के लिए है!!
सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की मजबूती के कारण कई प्रश्नों पर चर्चा हुई और कई प्रश्न उठाए गए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें एक संविधान पीठ बनाने की आवश्यकता है, जिसमें तर्क-वितर्क और प्रतिवाद के लिए बहुत समय लग सकता है। इस बीच, तमिलनाडु सरकार और उसके जैसे कई लोग नए मुख्यमंत्री पर विचार कर सकते हैं।
इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार विधेयकों और संबंधित शासन और कई विभागों के कामकाज पर काम करना बंद कर देती है। यह अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों के संघीय चरित्र के बिल्कुल खिलाफ है। भले ही निर्णय को पूरा करने में पूरा समय लग जाए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल एक 'सलाहकार राय' दे सकता है, जो राष्ट्रपति और स्वाभाविक रूप से सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।





